REPORT BY DR MUDITA POPLI
व्यापार मुसलमानों का पसंदीदा शगल रहा है भारतीय मुसलमान व्यापार में फल-फूल रहे है। मुरादाबादी पीतल के बर्तन, लखनऊ को चिकनकारी, भदोही के कालीन बनारस के साड़ी उद्योग से बड़ी संख्या में मुस्लिम कारीगर और निर्माता जुड़े हुए हैं। मुरादाबाद हमारे देश का ऐसा शहर है जहाँ बर्तनों का उद्योग बहुत पुराना है। यहाँ के बर्तनों की कई बड़ी-बड़ी फैक्ट्रियां है जहां कारीगर एक से बढ़कर एक खूबसूरत बर्तन बनाते हैं। मुरादाबाद के कारीगरों के बनाए बर्तन पूरी दुनिया में मशहूर हैं। इन बर्तनों में चाय कटोरे प्लेट, टोकरी और कई अन्य सामान शामिल हैं। यहां का बर्तन उद्योग बहुत प्रसिद्ध है और बहुत लोगों को रोजगार मिला हुआ है। कालीन विशेष रूप से भारत का एक महत्वपूर्ण उद्योग है। भारत में सबसे ज्यादा कालीन का काम जम्मू-कश्मीर और जयपुर में हैं। ईरान, चीन, भारत, पाकिस्तान, नेपाल और तुर्की कालीन उद्योग में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध है है। भारत दुनिया को 20 फीसद कालीन निर्यात करता है, अकेले जर्मनी में 40 फीसदी कालीन भारत से जाते हैं। वर्तमान में में एक लाख से अधिक करघे और 500 से अधिक इकाइया काम कर रही है। केंद्रीय कपड़ा उद्योग मंत्रालय ने 2001 में भारतीय कालीन प्रौद्योगिकी संस्थान की स्थापना की, जो उद्योग को बढ़ावा देने के लिए एशिया का एकमात्र संस्थान है। सरकार ने रॉ मैटेरियल प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित करने के लिए 8 करोड़ 68 लाख 70 हजार रुपये आवंटित किए हैं। अकेले मऊ के कपड़ा उद्योग को बढ़ावा देने के लिए 6.84 करोड़ की व्यवस्था की गई। एक प्रकार का कालीन ड्राइक है जो पूरी दुनिया में बहुत प्रसिद्ध था और इसकी कीमत अंतरराष्ट्रीय बाजार में 10 हजार से 50 हजार रुपये प्रति वर्ग मीटर तक हुआ करती थी। आज 200-300 प्रकार के कालीन है। उत्तरी भारतीय राज्य जम्मू और कश्मीर अपने हाथ से बुने हुए रेशमी कालीनों के लिए विश्व प्रसिद्ध है, जिनकी अंतर्राष्ट्रीय मांग बहुत अधिक हैं। कश्मीरी गलीचे पारंपरिक रूप से प्राच्य पुष्प डिजाइनों में बनाए जाते हैं. जिनमें आमतौर पर महत्वपूर्ण और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण रूपांकन शामिल होते हैं। 16वीं शताब्दी में कालीन हस्तकला फारस से कश्मीर घाटी पहुंची। सूफी संत असुन मक्का की तीर्थ यात्रा पर गए वापस लौटने पर उन्होंने फारसियों से कालीन बनाने की कला सीखी। डोगरा काल के दौरान उद्योग का विस्तार हुआ और कालीन ब्रिटिश और यूरोपीय बाजारों में पसंदीदा बन गए। श्रीनगर में हर दूसरे घर में कालीन बनाने के लिए कुटीर इकाई थी। जम्मू और कश्मीर के आर्थिक सर्वेक्षण की अनुसार 2011-2012 में कालीनों का कुल निर्यात 85 मिलियन डॉलर थी। लेकिन 2016 से 2017 मिलियन डॉलर रह गया।
उत्तर प्रदेश का मशहूर शहर लखनऊ अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। इस शहर ने एक तरफ अनीस और दबीर जैसे जाने-माने उर्दू शायर दिए हैं तो दूसरी तरफ लजीज व्यंजन दशहरी आम के साथ-साथ चिकन करी और जरदोजी को खूब बढ़ावा दिया है। नवाबों के जमाने से चला आ रहा चिकन उद्योग कहा जाता है कि मुगल बादशाह जहांगीर की बेगम नूरजहां के शासनकाल में चिकन का कारोबार शुरू हुआ था। इतिहासकारों का कहना है कि बादशाह जहांगीर के शासनकाल में उन्होंने इस कला के प्रचार-प्रसार के लिए माहौल तैयार करने में अहम भूमिका निभाई थी। चिकन कारी के कारोबार में लखनऊ के अलावा बाराबांकी, लखीमपुर खीरी, सीतापुर व आसपास के क्षेत्र के स्त्री-पुरुष जुड़े हुए हैं। इसके अलावा पश्चिम बंगाल, दिल्ली, जयपुर, हैदराबाद जैसे शहरों में कपड़े सजाने की कला के रूप में यह व्यवसाय खूब फल-फूल रहा है। इस व्यवसाय में छपाई, कढ़ाई, सिलाई, बुनाई, बटन बनाने वाले से लेकर धोबी तक शामिल है। लखनऊ अपने चिकन और जरदोजी कढ़ाई वाले कपड़ों के लिए पूरी दुनिया में मशहूर है। यहां बनने वाले कपड़े भारत के अलावा
सऊदी अरब, अमेरिका, सिंगापुर यूएई, यूके और अपने देश में कर्नाटक, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, राजस्थान, केरल, आंध्र प्रदेश आदि हर राज्य में पहुंचते हैं। चिकन के कपड़े बड़े फैशन शो की शोभा है। फिल्मी कलाकार आए दिन चिकन कढ़ाई वाले कपड़ों में नजर आते हैं। ईद, बकरीद , दीवाली जैसे महत्वपूर्ण त्योहारों के दौरान इसका कारोबार बहुत अच्छा होता है। लखनऊ के अनेक परिवार अपनी रोजी-रोटी के लिए चिकनकारी और जरदोजी के कारोबार पर निर्भर है। लखनऊ चिकन एसोसिएशन के संयोजक सुरेश पावलानी के मुताबिक भारतीय अर्थव्यवस्था में इस कारोबार की अहम भूमिका है। यह कारोबार सालाना करीब 300 करोड़ रुपये का है। चिकनकारी की तरह जरदोजी का बिजनेस भी काफी अहम है। विदेशों में इस -तरह के कपड़ों की लोकप्रियता बहुत अधिक है। अकेले उत्तर प्रदेश में 50,000 परिवारों के 2.50,000 लोग इस पेशे से जुड़े हैं, इसके अलावा कासगंज के 65,000 और ललितपुर के सैकड़ों लोग इस पेशे से जुड़े हैं, जो भारत की अवस्था के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
भारत के महत्वपूर्ण उत्पादों में से एक बनारसी साड़ी है। बनारसी साड़ियों को शादी की पोशाक माना जाता है। बनारसी साड़ी पुढी ,नक्की टिपिकल, इंटर ,तनछकोई बनारसी आदि कई वैरायटी में उपलब्ध है। यहां की साड़ियां बहुत मेहनत से तैयार होती है। पहले साड़ी सिर्फ हैंडलूम से बनती भी आधुनिक समय में हैंडलूम की जगह पावरलूम ने ले ली है, लेकिन बनारसी रेशम का उल्लेख सबसे पहले महाभारत और बौद्ध इतिहास में मिलता है। इतिहासकार कहते हैं कि इसे लाने का श्रेय मुगलों को जाता है, इसे बनाने और डिजाइन करने के लिए मुगलों ने हमेशा अपनी पीठ थपथपाई। कहा जाता है कि मुगलों ने इसके लिए कारीगर तैयार किए। बनारसी साड़ियों में ब्रोकेड और जरी का पहला जिक्र 19वीं सदी में मिलता है। कहा जाता है कि उस समय गुजरात के रेशम बुनकर भूखमरी के कारण बनारस में आकर बस गए थे, 17वी शताब्दी में यहीं से रेशम के ब्रोकेड का काम शुरू हुआ था। 18वीं और 19वीं सदी में यह बेहतर से बेहतर होता गया। बनारसी साड़ी उद्योग से लगभग 12 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। बनारसी साड़ी बनाने में सिल्क का इस्तेमाल होता है। बनारसी साड़ी का वजन आमतौर पर 400 से 500 ग्राम के बीच होता है भारी काम होने पर वजन एक किलोग्राम तक होता है। एक बनारसी साड़ी हजार से 2 लाख तक बिकती है। बनारसी साड़ियों के लिए प्रमुख बाजार बंगाल और बांग्लादेश हैं और जहाँ भी भारतीय महिलाएं मौजूद है. बनारसी साड़ियों का रिवाज हैं। सांसद के रूप में बनारस का प्रतिनिधित्व करने वाले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब से बनारस की संस्कृति और सभ्यता पर ध्यान केंद्रित किया है, तब से हस्तशिल्प को मजबूत करने की दिशा में बहुत कुछ किया गया है। यह बनारसी सिल्क और बनारसी शिल्प को एक नई पहचान दे रहा है। काशी कॉरिडोर के विकसित होने से बनारस में देशी-विदेशी पर्यटकों की संख्या दिन-ब-दिन बढ़ती जा रही है, इससे काशी के लोगों की अर्थव्यवस्था में और सुधार होगा और बनारसी साड़ियों और बुनकरों को पूरी दुनिया में काफी बढ़ावा मिलेगा। इसके अलावा भारत में तरह-तरह की साड़ियों का उत्पादन होता है, जिनमें से बांधनी साड़ी प्रसिद्ध है। मध्य प्रदेश में उत्पादित चंदेरी रेशम साड़ियों को उनकी सोने और चांदी की कढ़ाई के लिए जाना जाता है। इन साड़ियों में गोल्ड कॉइन मोटिफ्स और मोर डिजाइन मिलते हैं ये साड़ियां हैंडलूम पर तैयार होती है. यही इनकी खासियत है। असम की पारंपरिक मोंगा साड़ी भारत में प्रसिद्ध है।मोगा रेशम का उपयोग ज्यादातर असमिया महिलाएं पारंपरिक परिधान बनाने के लिए करती है। इस साड़ी की अच्छी बात यह है कि इस में हर जुलाई के बाद निखार आता है। तमिलनाडु के काधीपुरम क्षेत्र की रेशमी साड़ियां बहुत प्रसिद्ध है शहतूत रेशम के धागों से निर्मित कांजीवरम साड़ियाँ अपनी चमक और जटिल जरी के काम के लिए जानी जाती है। इस साड़ी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा पल्लू है जिसे अलग से बनाया जाता है और बाद में साड़ियों में जोड़ा जाता है। पेठनी साडियां नाजुक रेशमी धागों से बनी होती है, जिनके किनारों पर चिकने और चौकोर डिजाइन होते हैं, जिन पर मोर की आकृति या चौड़े प्रकाश वाले डिजाइन होते हैं। यह महाराष्ट्र की महिलाओं द्वारा पहने जाने की एक पारंपरिक शैली है। केंद्रीय वाणिज्य उद्योग मंत्रालय भारत सरकार बुनकरों, कारीगरों और हथकरघा उद्योग से जुड़े लोगों के लिए भी पूरे देश के हस्तशिला को पूरी दुनिया में पहचान दिलाने का प्रयास कर रहा है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के अनुसार, अकेले उत्तर प्रदेश ने अगले पांच वर्षों में अपने निर्यात को 1.25 लाख करोड़ रुपये से बढ़ाकर 7.25 लाख करोड़ रुपये करने का लक्ष्य रखा है। नि:संदेह उत्तर प्रदेश ने देश के निर्यात को बढ़ाने के लिए एक मॉडल बनने की अपनी क्षमता में वृद्धि की है। तटीय राज्यों को छोड़कर उत्तर प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक निर्यातक है। अगले पांच वर्षों में केंद्र सरकार के सहयोग से उत्तर प्रदेश के श्रमिकों उद्योगपतियों, निर्यातकों को रक्षा, रेलवे, मोबाइल, चिकित्सा में बड़ा निवेश मिलने की संभावना है।












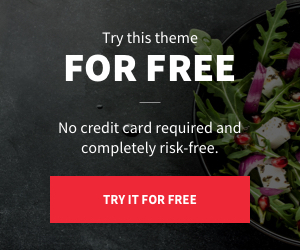

Add Comment