अनुसंधानकर्ता : एम एल गर्ग महानिरीक्षक
डा. सुरेंद्र शर्मा समन्वयक पांडुलिपि
आजकल के परिवेश में लोग श्राद्ध आदि कर्म को नही करते ना ही इसके महत्व को समझते हैं, हमारी ज्ञान राशि वेद में श्राद्ध का वैज्ञानिक वर्णन किया हैं जिसे ऋषियों ने अनुसंधान करके बताया है उसी क्रम में वेद वैज्ञानिक पंडित मधुसूदन ओझा जी ने पितृ समीक्षा में इस भाग को सिद्ध किया है साथ ही पंडित प्रवर सुरजन दास स्वामी ने श्राद्ध के रहस्य को बताया है, क्या है पितृ क्यों करना चाहिए श्राद्ध और उन पितरों का हमारी शरीर के बनने में क्या योगदान है इस अनुसंधान में स्पष्ट करने का प्रयास किया है।
दिव्यपितर, ऋतुपितर तथा प्रेतपितर भेद से पितर तीन प्रकार के है। इनमें श्राद्ध का सम्बन्ध प्रेतपितरों से है। दिव्यपितर और ऋतुपितर मनुष्यशरीर को उत्पन्न करते हुए कर्मभोग-लोकों में भोग कर लौटे हुए कर्मात्मा रूप भूतात्मा की मूर्तियोनि महान् आत्मा को उत्पन्न करते हैं, क्योंकि महानात्मा भूतात्मा से सम्बद्ध है। जैसा कि भगवान् मनु ने कहा है:
तावुभौ भूतसम्पृक्तौ महान् क्षेत्रज्ञ एव च। उच्चावचेषु भूतेषु स्थितं तं व्याप्य तिष्ठतः । । इति ।।
भूतात्मा से सम्बद्ध तथा उस पर अनुग्रहकर्ता यह महानात्मा मानवशरीर का परित्याग करने के बाद चान्द्रमस अर्थात् चन्द्रमा से सम्बन्धित होने के कारण चन्द्रमा में जाता है, जैसा कि कौषीतकि श्रुति में कहा है-
ये वै के चास्माल्लोकात् प्रयान्ति चन्द्रमसमेव ते सर्वे गच्छन्ति । तत इतो लोकात् प्रयन्तीति प्रेता उच्यन्ते ।।
अर्थात् जो मानव शरीरत्याग के बाद अन्य लोक में जाते हैं, वे चन्द्रमा में ही जाते हैं। इस मृत्यु लोक से प्रयाण करने के कारण “प्र इताः” इस व्युत्पत्ति से प्रेत कहलाते हैं। वे शरीर छोड़ने के समय जो चन्द्रमा की स्थिति है, उसके अनुसार ऊपरप्रयाण करते हुए तेरह नाक्षत्र मासों की पूर्ति होने पर चन्द्रमा में पहुँच जाते हैं। जिस ऋतु में मनुष्य की मृत्यु होती है वही ऋतु उसका चन्द्रलोक में स्वरूप बनता है। यदि वसन्त ऋतु में मरता है, तो वह वसन्तु ऋतु होता है और ग्रीष्म ऋतु में शरीर त्याग करता है, तो वह ग्रीष्मरूप हो जाता है। सापिण्ड्य रूप से ज्ञात अर्थात् 7 प्रकार के सपिण्ड मनुष्य पितर गान्धर्वशरीर धारण करके प्रेतपितर कहलाते हैं।
ये प्रेत पितर पर, अवर भेद से दो प्रकार के हैं पिण्डभाक् व लेपभाक्। पिण्डभाक् अवर पितर हैं ये अनुमुख हैं और लेपभाक् पर पितर हैं ये नान्दीमुख अर्थात् प्रसन्नमुख होते हैं। जैसा कि अभियुक्त कहते हैं
“ लेपभाजश्चतुर्थाद्याः पित्राद्याः पिण्डभागिनः । पिण्डदः सप्तमस्त्वेषां सापिण्डयं साप्तपौरुषम् ।।“
अर्थात् सात पितरों में पिता, पितामह, प्रपितामह ये तीन पितर पिण्डभाग हैं तथा वृद्ध प्रपितामह, अतिवृद्ध प्रपितामह, वृद्धातिवृद्ध पितामह ये तीन लेपभाग हैं। क्योंकि सन्तान में पितरों से प्राप्त होने वाली 56 कलाओं में से, पिता से 21 कलायें, पितामह से 15 कलायें, प्रपितामाह से 10 कलायें प्राप्त होती हैं। अतः इन तीनों पितरों से प्राप्त होने वाली कलाओं में सहोद्रव्य का आधिक्य है अतः सन्तान जब इन पितरों को श्राद्धान्न प्रदान करती है तब अधिक श्राद्धान्न वाला पिण्ड प्रदान करती है और वृद्ध प्रपितामाह से सन्तान पुरुष में 7 कलायें अतिवृद्धप्रपितामह से 3 कलायें और वृद्धातिवृद्धपितामह से 1 कला प्राप्त होती है। अतः इन पितरों से प्राप्त होने वाली कलाओं में सहोद्रव्य कम हैं। अतः इनको जब सन्तान पुरुष श्राद्धान्न प्रदान करता है, वह द्रव्य पिण्ड नहीं अपितु लेपमात्र है। श्राद्धान के आधिक्य में पिण्डशब्द तथा उसकी कमी में लेपशब्द का प्रयोग होता है। ये 56 कलायें सन्तान को शरीरोत्पत्ति में काम आती हैं, अतः इन्हें उत्पत्तिशिष्ट कहा जाता है, तथा सन्तान की उत्पत्ति के बाद एक नाक्षत्रमास में चन्द्रमा से शुक्र में 28 कलायें और प्राप्त होती है, वे 28 कलायें या 28 कलात्मक सहः पिण्ड उत्पन्नशिष्ट कहलाता है। इस तरह 84 सोमकलायें प्रतिपुरुष में रहती हैं। क्योंकि प्रत्येक पुरुष किसी का पुत्र भी है और किसी का वृद्धातिवृद्ध प्रपौत्र भी है। यही 84 कला वाला महानात्मा है। यह आज के विज्ञान ने भी सिद्ध किया है जिसका अनुसंधान हमारे ऋषियों द्वारा पूर्व में ही किया जा चुका है प्राचीन पांडुलिपियों से इस भारतीय विज्ञान को जाना जा सकता है।













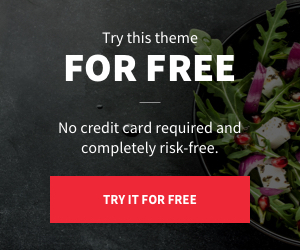

Add Comment